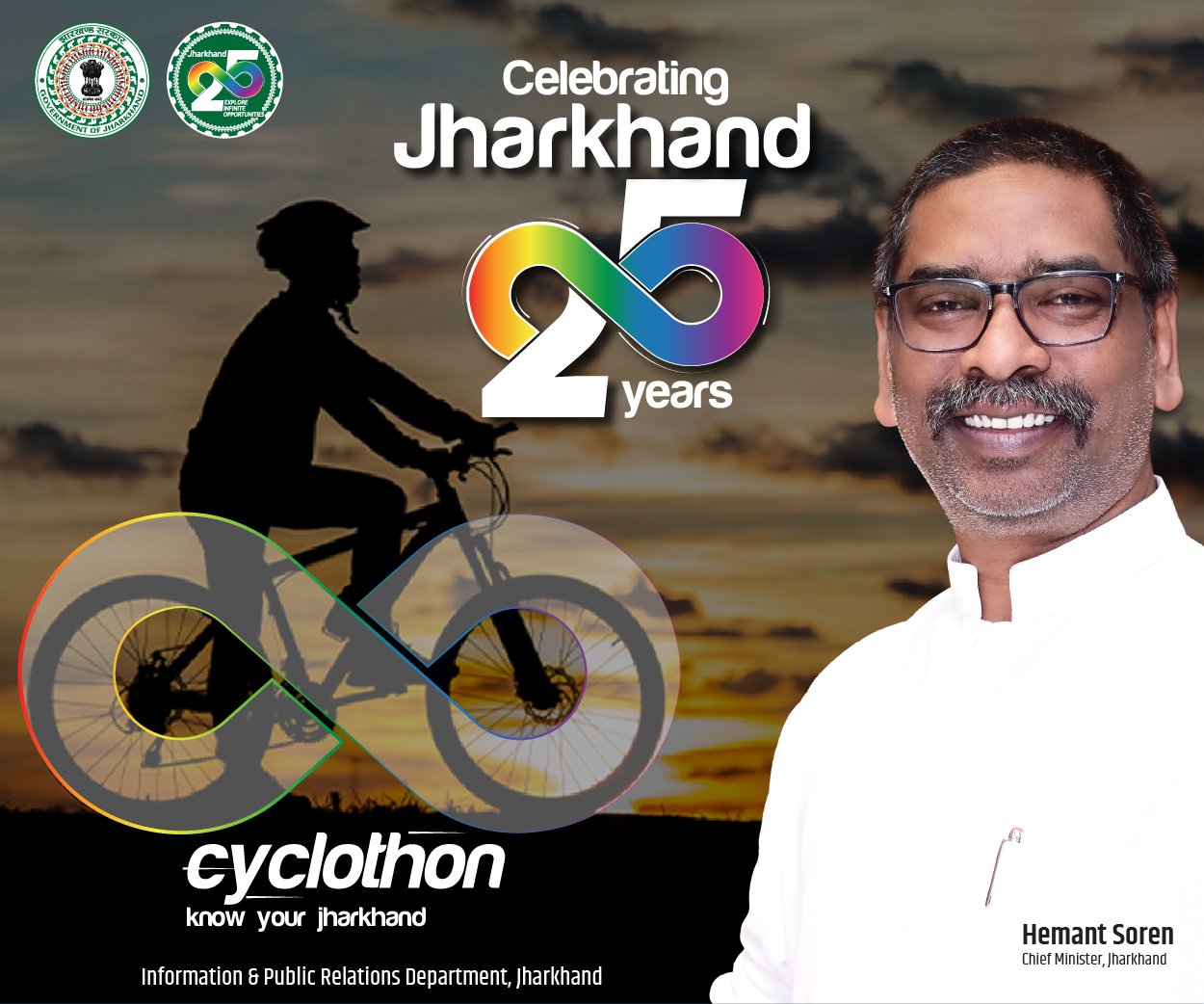RAJAT ALVI
सोरंडा के घने साल के जंगल में एक खुली जगह पर ग्राम सभा की बैठक चल रही है। पेड़ों की छाँव में बैठे आदिवासी उत्साह और चिंता के बीच बातें कर रहे हैं, “अब हमारे जंगल का कार्बन भी बिकेगा!” पहले लकड़ी, बाँस और तेंदूपत्ता बिकते थे, अब पेड़ों में जमा कार्बन को भी संपत्ति कहा जा रहा है। किसी के चेहरे पर उम्मीद की झलक है — “शायद इससे आमदनी बढ़ेगी।” तो किसी को डर है — “कहीं यह जंगल पर नया कब्ज़ा तो नहीं?” झारखंड की यह नई कहानी हरियाली, विकास और बाजार की एक जटिल गठजोड़ को बयां करती है।
झारखंड का हरित सपना अब धीरे-धीरे हकीकत बन रहा है। पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा एशिया का सबसे बड़ा साल वन माना जाता है, जहाँ के आदिवासी समुदाय—हो, मुंडा, बिरहोर, भूमिज—सदियों से जंगल को अपनी माँ की तरह पूजते आए हैं। यही जंगल अब “कार्बन भंडार” कहलाने लगे हैं। हाल के सरकारी और शोध अध्ययनों के अनुसार झारखंड के जंगलों में लगभग 246 मिलियन टन कार्बन जमा है। यह कार्बन न केवल पेड़ों में, बल्कि मिट्टी और पौधों में भी जमा रहता है, जो धरती के तापमान को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाता है।
राज्य सरकार की “बिरसा हरित ग्राम योजना” इसी हरियाली को नई दिशा दे रही है। इस योजना के तहत बंजर ज़मीनों पर फलदार और इमारती पेड़ लगाए जा रहे हैं, और ग्रामीणों को ‘कार्बन फाइनेंस’ से जोड़कर हर पेड़ से आय का नया स्रोत देने की कोशिश हो रही है। अब तक 18 जिलों के 30,000 से अधिक परिवार इस योजना से जुड़े हैं। यदि यह योजना ग्राम सभाओं की भागीदारी, पारदर्शिता और अधिकारों के साथ लागू की जाए, तो यह आदिवासी समुदायों के लिए हरियाली से रोज़गार और आय का अवसर बन सकती है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है—जंगल किसका है? और क्या सचमुच हवा भी बिक सकती है? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आधुनिक तो है, पर इसका मूल “हवा का व्यापार” है। बड़ी कंपनियां अपनी कार्बन उत्सर्जन सीमा से कम उत्सर्जन कर ‘कार्बन क्रेडिट’ कमाती हैं, और जो ज्यादा उत्सर्जन करती हैं, वे इन्हें खरीदती हैं। यानी एक कंपनी पेड़ लगाकर पर्यावरण प्रेमी कहलाती है, जबकि दूसरी कंपनी कोयला जलाकर उद्योग चलाती रहती है। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर इस कार्बन क्रेडिट व्यापार को वैधानिक रूप दिया है, जिससे कंपनियां सीधे ग्राम सभाओं या वन समुदायों से ‘कार्बन अधिकार’ खरीद सकती हैं।
यहाँ से कहानी पेचीदा हो जाती है। झारखंड के जंगल केवल संसाधन नहीं, बल्कि संस्कृति और आत्मा हैं। पेसा (1996) और वनाधिकार कानून (2006) ग्राम सभा को अपने जंगल और ज़मीन पर निर्णय लेने का अधिकार देते हैं, पर कार्बन व्यापार की नीतियों में इन कानूनों का जिक्र नहीं है। यदि किसी कंपनी ने ग्राम सभा से “कार्बन अधिकार” खरीद लिए, तो जंगल की निगरानी ड्रोन, उपग्रहों और बाहरी एजेंसियों के हाथों में चली जाएगी, और ग्राम सभा का अधिकार केवल काग़ज़ी दस्तावेज़ तक सीमित रह जाएगा। जंगल, जो कभी जीवन का हिस्सा था, अब केवल “कार्बन स्टॉक” बन जाएगा—एक सौदा, एक गिनती।
झारखंड में तीन लाख से अधिक वनाधिकार दावे अभी भी लंबित हैं। ऐसे में “कार्बन बेचने” का मतलब है बिना स्वामित्व के अपनी ही संपत्ति को गिरवी रखना। परियोजनाओं से जो धन आएगा, वह अक्सर गाँव तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि बीच में एजेंसियाँ, सलाहकार और कंपनियाँ अपना हिस्सा निकाल लेंगी। यही डर सारंडा के लोगों में भी गहराता है।
सारंडा सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा है। यहाँ के लोग महुआ, साल के पत्ते, झरनों का पानी, औषधियाँ और त्योहार—सब कुछ जंगल से ही पाते हैं। सरकार इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की तैयारी कर रही है, ताकि हाथियों का कॉरिडोर और जैव विविधता सुरक्षित रहे। पर जब इसे कार्बन व्यापार से जोड़ा जाता है, तो “हरित बाज़ार” का असली चेहरा दिखता है। अभयारण्य बनने के बाद लोगों के प्रवेश और उपयोग पर सख्त रोक लग सकती है—महुआ तोड़ने, लकड़ी लाने या औषधीय पौधे चुनने के अधिकार सीमित हो सकते हैं। कहने को यह पर्यावरण की रक्षा है, लेकिन असल में यह जंगलों पर नियंत्रण का नया रूप भी हो सकता है, जिसमें असली संरक्षक, यानी आदिवासी समुदाय, किनारे हो जाएंगे।
वैश्विक स्तर पर भी ऐसी योजनाओं का अनुभव मिल चुका है। केन्या, पेरू और ब्राजील जैसे देशों में स्थानीय समुदायों ने कहा है कि उन्हें कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं से न तो पर्याप्त मुनाफ़ा मिला, न ही जंगल पर निर्णय का अधिकार। कई बार लाभ केवल बाहरी कंपनियों और एजेंसियों के हाथ में रहा। ऐसे उदाहरण झारखंड के लिए चेतावनी हैं कि बिना सशक्त स्थानीय भागीदारी के यह प्रयास विकृत हो सकते हैं।
झारखंड के आदिवासी समाज ने कभी कार्बन की गणना नहीं की। उनका जीवन ही कार्बन न्यूट्रल था क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखा। अब वही समुदाय ‘कार्बन उत्पादक’ कहलाएगा और हवा किसी कंपनी की संपत्ति बन जाएगी। यह सिर्फ जंगल का मुद्दा नहीं, बल्कि न्याय का सवाल है—क्या हवा बेची जा सकती है? क्या जंगल का आशीर्वाद बाज़ार में तौला जाएगा?
यदि इस योजना को सच में ग्राम सभा के अधिकार, पारदर्शिता और भागीदारी के साथ लागू किया जाए, तो इसे कई सकारात्मक तरीकों से आगे बढ़ाया जा सकता है:
• ग्राम सभा को कार्बन क्रेडिट की निगरानी और लाभ वितरण समिति में मुख्य भूमिका देनी चाहिए।
• स्थानीय कार्बन रजिस्ट्री (community carbon registry) बनाकर पारदर्शिता बढ़ाई जाए।
• पर्यावरणीय NGOs और शोध संस्थान परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी करें।
• सरकार लंबित वनाधिकार दावों का त्वरित निपटारा करे, ताकि स्वामित्व स्पष्ट हो।
इस तरह न केवल जंगल और पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार और आय का स्थायी स्रोत भी बन सकेगा।
सारंडा के जंगल की गहराई में बसती है झारखंड की संस्कृति, आस्था और पहचान। हर पेड़, हर झरने की कहानी है, जो सदियों से आदिवासियों के जीवन का हिस्सा रही है। हवा, पानी और जंगल सभी की साझा धरोहर हैं। अगर कार्बन क्रेडिट जैसे आधुनिक औजारों को ग्राम सभाओं के अधिकार, पारदर्शिता और न्याय के साथ जोड़ा जाए, तो यह सच में हरित विकास का रास्ता खोल सकता है। नहीं तो यह “हरित विकास” नहीं, बल्कि “हरित विस्थापन” बन जाएगा। हवा सबकी है, और इसका मालिक वही होना चाहिए, जिसने उसे सबसे सच्चे दिल से सँभाला है—झारखंड का जंगल और इसके रखवाले।